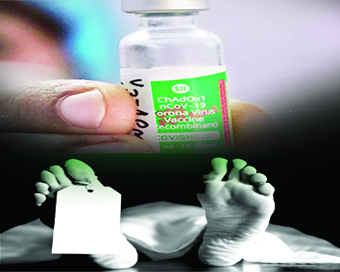भारत का विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र वैश्विक स्तर पर तेजी से उभर रहा है। इसकी स्थिति में निरंतर सुधार देखा जा रहा है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक-2021 में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया जबकि चीन पहले स्थान पर रहा।
इस रैंकिंग से पता चलता है कि अमेरिका और एशिया-प्रशांत क्षेत्र की तुलना में मैन्युफैक्चर्स भारत को पसंद कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यह इंडेक्स यूरोप, अमेरिका तथा एशिया-पैसेफिक (एपीएसी) के 47 देशों में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए आकषर्क या प्रॉफिटेबल डेस्टिनेशन की रैंकिंग करता है।
वर्तमान में विनिर्माण क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में 17% और 27.3 मिलियन से अधिक श्रमिकों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि में अभिन्न स्तंभ के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी) के अनुसार, भारत का लक्ष्य 2025 तक अर्थव्यवस्था के उत्पादन का 25% विनिर्माण से प्राप्त करना है। भारत में 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के सामान निर्यात करने की क्षमता है, और इस प्रकार यह प्रमुख वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की राह पर है। ‘मेक इन इंडिया’, ‘प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना’, और ‘उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना’ जैसी नीतियों ने विनिर्माण क्षेत्र को सशक्त किया है।
सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अन्य बहुत-सी योजनाएं भी बनाई हैं। इस क्षेत्र में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए कई विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भी स्थापित किए हैं। घरेलू विनिर्माण ईकोसिस्टम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग महत्त्वपूर्ण है, इसके लोकलाइजेशन के लिए नये सिरे से स्कीम बनाई जा रही है। इससे चीनी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में स्थानीय निर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में संभावित रूप से सुधार करने में मदद मिलेगी। ग्लोबलाइज्ड सप्लाई चेन और बढ़े हुए भू-राजनीतिक जोखिमों की दुनिया में उनकी बारगेनिंग पावर भी बढ़ेगी। विनिर्माण क्षेत्र में कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में बदला जाता है। यह क्षेत्र विशेष रूप से श्रम आधारित है। इसमें मशीनरी, औजार और श्रम का इस्तेमाल किया जाता है। मगर विगत वर्षो में इसकी गति अपेक्षाकृत धीमी रही है।
विनिर्माण क्षेत्र में यद्यपि उत्पादन बढ़ा है, लेकिन विश्लेषक इसे नाकाफी बताते हैं। उनका मानना है कि बुनियादी ढांचे का अभाव, कुशल श्रम की कमी और ऋण प्राप्त करने की कठिनाइयां, व्यापार नीति में निरंतरता का अभाव और जटिल कानूनी प्रावधानों तथा शैक्षणिक एवं कौशल व्यवस्था की अपर्याप्तता आदि सभी इसको प्रभावित करते हैं। जमीन अधिग्रहण से लेकर बिजली पर आने वाले खर्च और तमाम मंजूरियां हासिल करने में लगने वाले वक्त से लेकर माल ढुलाई (लॉजिस्टिक) की लागत और कर विवाद आदि के कारण भारत देसी-विदेशी विनिर्माण कंपनियों के लिए सही जगह नहीं बन पाया है। यह क्षेत्र वैश्विक मांग में कमी और चीन जैसे देशों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भी प्रभावित हुआ है।
चीन दुनिया में सबसे बड़ी विनिर्माण एवं व्यापारिक शक्ति बन चुका है। चीन 1 लाख करोड़ डॉलर से अधिक व्यापार अधिशेष (ऐसी स्थिति जब कोई देश आयात से अधिक निर्यात करता है) की स्थिति में है, जो बेमिसाल आंकड़ा है। मगर ट्रंप के सत्ता में दुबारा लौटने के बाद जिस प्रकार से चीन के साथ उसका टैरिफ वॉर चल रहा है, उसके मद्देनजर बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि चीन के उत्पादों का पश्चिमी देशों के बाजार में पहुंचना बंद हो जाएगा तो वे कहां जाएंगे? चीन तो इन उत्पादों का उत्पादन बंद नहीं करेगा क्योंकि यह उसकी अर्थव्यवस्था के लिए घातक होगा और अपस्फीति का जोखिम बढ़ जाएगा।
लिहाजा, चीन की अधिकांश कंपनियों के लिए निर्यात प्राथमिकता रहेगी। चीन से ये उत्पाद भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में धकेले जाएंगे। ऐसे में विकासशील देशों के लिए जोखिम यह है कि चीन में तैयार उत्पाद उनके बाजारों में आने से वे अपना औद्योगिक ताना-बाना सुरक्षित रखने और आकार एवं दक्षता बढ़ाने के लिए संघर्ष करेंगे। इस खतरे की आशंका अधिक है कि चीन इन देशों में स्थानीय औद्योगिक आधार को कमजोर कर देगा जिससे वे आकार, लागत एवं तकनीक के मोर्चे पर चीन की औद्योगिक ताकत का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें चीन से आने वाली वस्तुओं से निपटने की रणनीति तैयार करने और बेहतरीन एवं उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करने के लिए अपने उद्योगों को सतर्क करना होगा और औद्योगिक गतिविधियों में कमी आने से रोकने और आपूर्ति व्यवस्था सुरक्षित रखने के लिए जरूरी उपाय करने होंगे।
यह भी गौर करने योग्य है कि अभी दूरसंचार सुविधाएं मुख्य रूप से बड़े शहरों तक ही सीमित हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण तक अनुकूल पहुंच की कमी और कार्यशील पूंजी की उच्च लागत भी एक बड़ी बाधा बनी हुई है। इसके अतिरिक्त, कमजोर या खराब आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से इस क्षेत्र की लागत में वृद्धि होती है। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार, उद्योग जगत, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों आदि सभी हितधारकों के स्तर से मिले-जुले प्रयासों की आवश्यकता है।
| गिरीश पाण्डे |
Tweet





__1734805153.jpg)